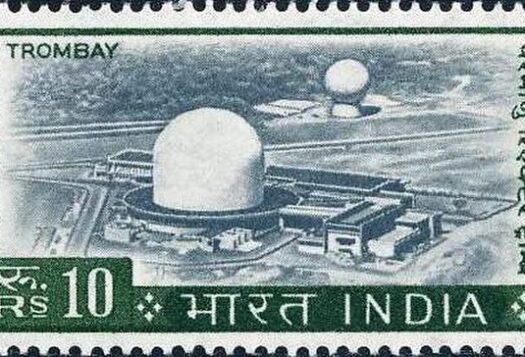हाल ही के सऊदी-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते (एसएमडीए) की घोषणा ने कई पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया। भारत में, इस घटनाक्रम को प्रारम्भ में, दक्षिण एशिया के दृष्टिकोण से देखा गया, तथा एक प्रारंभिक “इस्लामिक नाटो” या मुस्लिम देशों के सामूहिक सैन्य गठबंधन की चर्चा उभरी, जिसके नई दिल्ली के लिए गंभीर से अति गंभीर निहितार्थ हैं। इस व्याख्या को पश्चिम एशिया पर नज़र रखने वाले अनुभवी विशेषज्ञों और राजनयिकों ने सूक्ष्म रूप से समझा और तर्क दिया कि – यह समझौता पश्चिम की ओर उन्मुख है, क़तर के भीतर इज़राइल के अकारण हमलों से प्रेरित है, और इसका भारतीय हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा| उन्होंने इस दावे के प्रमाण के रूप में पिछले दो दशकों में नई दिल्ली के रियाद के साथ बढ़ते संबंधों की ओर भी इंगित किया।
हालाँकि, इस समझ के बावजूद, यह अपेक्षा करने के यथोचित कारण हैं कि इस समझौते और सऊदी-पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ सुरक्षा संबंधों का व्यापक भारत-पाकिस्तान रणनीतिक प्रतिस्पर्धा – विशेषकर, पाकिस्तान से अलग होने के भारत के प्रयासों पर, हल्के से मध्यम प्रभाव पड़ेगा। ऐसा पाकिस्तान के अपने समझौतों के दायरे से बाहर जाकर गठबंधनों का लाभ उठाने के इतिहास, मध्य पूर्व में सऊदी अरब की असुरक्षा को बढ़ाने वाले मौजूदा रुझानों और भारत पर पाकिस्तान के निरंतर रणनीतिक ध्यान के कारण है।
गठबंधन निर्माण के प्रति पाकिस्तान का दृष्टिकोण
एक दुर्बल शक्ति के रूप में, जो संशोधनवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भरोसा रखता है, तथा रणनीतिक गहराई की कमी से जूझ रहा है, पाकिस्तान लंबे समय से भारत के साथ अपनी विषमताओं को दूर करने के लिए क्षेत्र के बाहर के बाह्य महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को विकसित करने की चेष्टा कर रहा है। उदाहरण के लिए, शीत युद्ध के प्रारंभिक चरण में, पाकिस्तान ने सोवियत संघ को नियंत्रित करने के अमेरिकी लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपने भौगोलिक लाभों की प्रस्तुति कर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन स्थापित किया। परंतु, साम्यवाद-विरोध पाकिस्तान के अधिक स्थायी उद्देश्य: दक्षिण एशिया में भारतीय शक्ति को नियंत्रित करने के लिए भू-राजनीतिक रूप से सुविधाजनक आवरण मात्र था। सोवियत-अफ़ग़ान युद्ध के दौरान, इस्लामाबाद ने आधुनिक हथियार प्राप्त करने के साथ साथ, भारत को ध्यान में रखते हुए परमाणु हथियार निर्मित करने हेतु अमेरिका और सऊदी अरब पर इसी प्रकार की निर्भरता का लाभ उठाया|
“यह अपेक्षा करने के यथोचित कारण हैं कि इस समझौते और सऊदी-पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ सुरक्षा संबंधों का व्यापक भारत-पाकिस्तान रणनीतिक प्रतिस्पर्धा—विशेषकर, पाकिस्तान से अलग होने के भारत के प्रयासों पर, हल्के से मध्यम प्रभाव पड़ेगा।”
2000 के दशक के प्रारम्भ में जब वाशिंगटन के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने ग्वादर बंदरगाह को एक नए आर्थिक और संभावित रणनीतिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर, बीजिंग को आकर्षित करने की चेष्टा की। उन्होंने हिंद महासागर तक चीन की पहुँच की आवश्यकता का लाभ उठाते हुए इस परियोजना में उसे एक हितधारक के रूप में शामिल करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेताओं ने यह प्रस्ताव इस उम्मीद के साथ दिया था कि भविष्य में भारत के विरुद्ध यह बंदरगाह लाभदायक सिद्ध होगा। जैसा कि मुशर्रफ़ ने एक दशक से भी अधिक समय बाद स्पष्ट किया, “ग्वादर पूर्ण रूप से मेरा विचार था, चीन का नहीं। मुझे केवल पाकिस्तान के सामरिक हितों की चिंता थी,”उनका संकेत पाकिस्तान के उस लंबे समय से चले आ रहे भय की ओर था कि भारत कराची बंदरगाह को अवरुद्ध कर देगा। उनके अनुसार, ग्वादर पाकिस्तान को मध्य पूर्व के तेल तक भारत की पहुँच को ख़तरे में डालने और इस तरह उसकी प्रतिरोधक (deterrence) क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकता था। हालाँकि, प्रारम्भ में चीनी नेताओं को इस परियोजना के महत्त्व पर संदेह था, लेकिन अंततः उन्होंने इस परियोजना पर स्वीकृति जताई और समय के साथ, जैसा कि विद्वान डैनियल मार्के बताते हैं, पीएलएएन ने बंदरगाह के रणनीतिक लाभों की सराहना करना प्रारम्भ कर दिया। पाकिस्तान और चीन के बीच साझा सुरक्षा हितों की यह भावना पिछले कुछ वर्षों से विकसित हुई है, जिसे विशेषज्ञ समीर लालवानी “चौखटीय गठबंधन” का नाम देते हैं। भारत ने इस बढ़े हुए सुरक्षा सहयोग का प्रभाव इस वर्ष महसूस किया, जब मई में पाकिस्तान ने अपने चार दिवसीय गतिज संघर्ष में चीनी-निर्मित प्लेटफार्मों का प्रयोग किया।
एक चौथाई सदी के उपरांत, भारत पुनः देख रहा है कि कैसे एक प्रबल आर्थिक साझेदार अपने मूल सुरक्षा हितों की पूर्ति हेतु पाकिस्तान पर निर्भर हो रहा है। सऊदी अरब जहाँ ईमानदारी से भारत को यह संदेश देना चाहता है कि उसके हितों की रक्षा की जाएगी, वहीं नई दिल्ली में एक तरह की पूर्वानुभूति उभर रही है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान अपने गहरे होते राजनैतिक संबंधों का लाभ ऐसे तरीक़ों से उठा रहा है जो भारतीय हितों के लिए नुक़सानदेह हो सकते हैं—ख़ासकर भविष्य में किसी संभावित संकट की स्थिति में।
मध्य पूर्व में वर्तमान रुझान एवं पाकिस्तान की विनिमयशीलता
तथापि भारत में कुछ लोगों के लिए एसएमडीए के संचालकों के बारे में दक्षिण एशिया-केंद्रित दृष्टिकोण रखना आकर्षक हो सकता है, परन्तु इस समझौते को मध्य पूर्व की भू-राजनीति के संदर्भ में देखना लाभदायक है| रियाद के लिए, सुरक्षा चिंता के स्रोत प्रबल एवं संरचनात्मक हैं| यमन और ईरान के बीच सुधरते संबंधों, इज़राइल की बढ़ती अनिश्चिताओं, और क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था के आंशिक रूप से बिखरने के मध्य में, वाशिंगटन के संभावित रूप से मद्धिम होती सुरक्षा आश्वासनों के बावजूद—अमेरिका यमन में हूतियों के कारण चिंताग्रस्त है| ट्रम्प व्हाइट हाउस ने, अपनी ओर से, मध्य पूर्व सहित विदेशों में संघर्ष क्षेत्रों में अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को घटाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जहाँ से अमेरिकी सैन्य कर्मियों और उपकरणों की छोटे पैमाने पर वापसी पहले से ही चल रही है।
दीर्घावधि में, यह स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मध्य-पूर्व सुरक्षा की नई क्षेत्रीय संरचनाओं का समर्थन करने का औचित्य पैदा करती है, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है| यह बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ते वैश्विक रुझान के अनुरूप ही होगा- जिसका भारत ने सैद्धांतिक रूप से वर्षों से समर्थन किया है। अमेरिका ने आखिरी बार 1970 के दशक में साम्राज्यवादी अतिरेक को रोकने और रणनीतिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए ऐसे “क्षेत्रीय शेरिफ़”-समर्थक नवाचारों, या “दायित्व एक दूसरे पर डालने” के प्रयासों की कोशिश की थी। तीव्र गति से, बहुध्रुवीय होते विश्व में, पाकिस्तान की अधिक इच्छुक और सक्षम सैन्य संपत्तियों और कर्मियों का इस्लामाबाद कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है, और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है।
दरअसल, सऊदी-पाकिस्तान एसएमडीए संकट के दौरान मध्य पूर्व की सुरक्षा संरचना में इस्लामाबाद की भूमिका का दूसरा उदाहरण है: इज़राइल के दोहा हमलों से पूर्व, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर उन नेताओं में शामिल थे, जिनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने जून में अपने व्हाइट हाउस दौरे के समय 12-दिवसीय ईरान-इज़राइल युद्ध पर चर्चा की थी। यह तब हुआ जब ईरानी अधिकारी दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार से ईरान को परमाणु हमलों से बचाने की प्रस्तुति कर रहा है—एक ऐसा दावा जिसका पाकिस्तानी सांसदों ने दृढ़ता से खंडन किया।

इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान ने संघर्ष क्षेत्रों में सैन्य ज्ञान के एक माध्यम के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। चीन और तुर्की जैसे परिपक्व रक्षा औद्योगिक परिसरों वाले देशों द्वारा निर्मित हथियारों और प्रणालियों के साथ पाकिस्तान का गहरा एकीकरण, उसे ऐसे उपकरण और ज्ञान तीसरे देशों को प्रदान करने में उन देशों को सक्षम बनाता है, जिनके पास तुलनात्मक रूप से स्वदेशी क्षमताएँ नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अज़रबैजान जैसे देशों के लिए पाकिस्तान का महत्त्वपूर्ण रक्षा श्रेणी उसे सऊदी अरब के साथ भी ऐसा ही प्रतिमान अपनाने का अवसर देता है, जिसकी उन्नत रक्षा प्रणालियों के उत्पादन की स्वदेशी क्षमता अभी प्रारम्भिक चरण में है। यदि यह एकीकरण और प्रगाढ़ होता है, तो इससे चीन से सऊदी अरब और अज़रबैजान होते हुए तुर्की तक हथियारों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए सहयोग का एक प्रभावी क्षेत्र उद्यत होगा।
इस संदर्भ में, पहल करने वाले नेतृत्व के तहत, तीव्रता से सक्षम होती पाकिस्तानी सेना सुरक्षा समाधानों के एक पुक्ता विकल्प के रूप में उभर रही है—जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के हिस्से के रूप में ग़ाज़ा में पाकिस्तानी कर्मियों को तैनात करने की संभावना भी सम्मिलित है। विदेशों में सुरक्षा सहायता लक्ष्यों में भाग लेने का पाकिस्तान का अनुभव और उसकी इच्छाशक्ति, मध्य पूर्व में अरबों की नई सुरक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है और साथ ही कम अनुभवी सैन्य बलों की तैनाती से होने वाले जोखिमों के प्रति अरबों की विरुचि को भी कम कर सकती है। ऐसे रुझान आसानी से या जल्द ही दुर्बल होने की संभावना नहीं रखते हैं—जिसका यथार्थ है कि रियाद के मुक़ाबले पाकिस्तान की स्थिति स्थिर और मजबूत वास्तव में विकसित हुई है। भविष्य में, किसी संघर्ष में, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान इस ताक़त का प्रयोग किस प्रकार से करेगा, यह पहले से तय करना कठिन हो सकता है। फिर भी, गठबंधन के इस संभावित परिपक्व होने से रियाद और अन्य खाड़ी देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की प्रासंगिकता को कम करने के पिछले दो दशकों के भारत के अथक प्रयासों पर पानी फिरने का ख़तरा मंडरा रहा है।
पाकिस्तान का भारत पर निरंतर ध्यान
हाल ही में, मध्य पूर्व में अपनी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, इस्लामाबाद की मुख्य रणनीतिक चिंता भारत के साथ उसके संबंध ही बने हुए हैं। मई में चार दिनों तक चले संघर्ष की समाप्ति के बाद से, पाकिस्तान ने भारत से जुड़ी अपनी कूटनीति और सैन्य प्रयासों को इस आशंका से तेज़ कर दिया है कि संघर्ष पुनः हो सकता है; पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि “भारत के साथ युद्ध की संभावनाएँ वास्तविक हैं।”
बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान की विद्यमान मुद्रा और उसका नेतृत्व, भारत के उभरते दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए, क़तर पर इज़राइली हमलों के उपरांत, हाल ही में हुए दोहा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क़तर के विरुद्ध इज़राइल की कार्यवाही, और पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की कार्यवाही के बीच तुलना करना प्रतीत होता है। पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान को संभवतः यह अपेक्षा है—और यह अपेक्षा बेवजह नहीं है—कि इज़राइल के मामले में खाड़ी और अरब देशों के साथ उसकी एकजुटता को कश्मीर मुद्दे से जोड़ा जाएगा। इन विचारों की प्रस्तुति, पाकिस्तान के अनुसार उसके पक्ष में, भविष्य में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान, या सिंधु जल संधि के भारत द्वारा संभावित उल्लंघन (ऐसी कार्यवाही जिसे इस्लामाबाद युद्ध की कार्यवाही मानता है) पर प्रतिक्रिया देते समय की जाएगी जब उसकी अरब देशों के साथ एकजुटता को सकारात्मक रूप से स्मरण किया जाएगा |
इस संदर्भ में, भारत को “डी-हाइफ़नेशन” की चुनौतियों का पुनः प्रवर्तन दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली ने पिछले एक दशक में अरब देशों की भारत के प्रति विदेश नीतियों में आए परिवर्तनों पर नज़र रखी है, और इस प्रकार के घटनाक्रमों को—विशेषकर, रियाद द्वारा कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय मामले के रूप में दिल्ली की व्याख्या को स्वीकृति प्रदान करना—भारत के “डी-हाइफ़नेशन” माना गया है।
“कम से कम, भारत खाड़ी देशों की राजनैयिक तटस्था या अगले भारत-पाकिस्तान संकट या संघर्ष में रियाद की स्थिति पर संसय है।”
अब एसएमडीए का उभरता स्वरूप क्षेत्रीय स्तर पर भारत की तरफ़ सऊदी अरब के रूख पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह रियाद के हाल ही की भारत-पाकिस्तान संकट में मध्यता की भूमिका को ठेस पहुँचा सकता है जो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का पक्षधर रहा है। कम से कम, भारत खाड़ी देशों की राजनैयिक तटस्था या अगले भारत-पाकिस्तान संकट या संघर्ष में रियाद की स्थिति पर संसय है।
भारत को क्या करना चाहिए?
एसएमडीए, रियाद द्वारा नई दिल्ली की संवेदनशीलताओं और हितों की अनदेखी करने का उदाहरण कम, बल्कि, रियाद द्वारा अपने देश के निकट बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर अधिक केंद्रित है| न तो नई दिल्ली के पास अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए रियाद से नाराज़ होने का कोई कारण है, न ही रियाद को बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ 1.4 अरब लोगों की बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ संबंधों को ख़राब करने में कोई रुचि है; विशेष रूप से तब जब रूसी तेल से दूर होकर पुनः विविधीकरण करने की भारत की बढ़ती आवश्यकता भी खाड़ी देशों के साथ पुनर्जीवित ऊर्जा संबंधों की ओर संकेत करती है।
हालाँकि, भारत-सऊदी संबंधों में सुधार एक अधिक स्थिर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। वह व्यवस्था अब तेज़ी से बदल रही है, और पुराने आश्वासन अब पक्की ज़मानत नहीं रहे। हाल के घटनाक्रमों की दृष्टि में, भारत को 2010 और 2020 के प्रारम्भिक वर्षों में प्राप्त की गई की गई कूटनीतिक और प्रतिष्ठागत बढ़त को बरकरार रखने के लिए सावधानी से क़दम उठाने होंगे।
इसलिए, जबकि भारत को इस समझौते को मुख्य रूप से मध्य पूर्व से संबंधित मानना चाहिए, परंतु, उसे समय के साथ-साथ, खाड़ी देशों के संबंध में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव की संभावना के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए, जो संकट के समय में भारतीय हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं| इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, नई दिल्ली को खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को प्रबलता प्रदान करने में निवेश करना होगा। इसमें आर्थिक संबंधों में तीव्रता लाना सम्मिलित हो सकता है, जो खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के लिए एक प्रेरक के रूप में पहले ही अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं| साथ ही, भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भी सम्मिलित हो सकता है, ताकि सऊदी-पाकिस्तान समझौते और भारतीय हितों के बीच एक उभयरोधी निर्मित किया जा सके।
This article is a translation. Click here to read the original in English.
Views expressed are the author’s own and do not necessarily reflect the positions of South Asian Voices, the Stimson Center, or our supporters.
***
Image 1: MEAphotogallery via Flickr
Image 2: S. Jaishankar via X