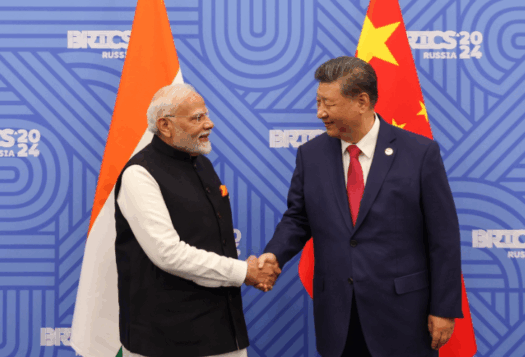चार दिनों तक प्रक्षेपास्त्र हमलों, ड्रोन घुसपैठ और तीव्र हवाई युद्ध वाले संघर्ष के उपरांत, भारत और पाकिस्तान 10 मई को युद्ध विराम के लिए मान गए। दोनों देशों ने इस संघर्ष में अपनी-अपनी जीत मानी और एक-दूसरे से निपटने के अपने नए तरीकों का जश्न मनाया। यद्यपि दुनिया को यह बात सामान्य लगे, पर इस झड़प के पूर्ण युद्ध में परिवर्तित होने का ख़तरा 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से इतना अधिक कभी नहीं रहा, जब दोनों देश परमाणु-हथियार राष्ट्र बने थे।
जबकि दोनों पक्ष संकट से पीछे हट चुके हैं, भारत के दृष्टिकोण से यह युद्ध विराम सशर्त है और भारत के नेता इस बात पर बल देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हालाँकि यह अधरझूल की स्थिति है, विचारणीय यह है कि हम इस स्थिति में पहुँचे कैसे और भारत के लिए इस स्थिति से उसकी पाकिस्तान नीति में बदलाव क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
भारत द्वारा “नए सामान्य” की खोज के पीछे तर्क
2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के उपरांत, भारत में यह समझ बढ़ी कि नैतिकता और कूटनीतिक विरोध अकेले पाकिस्तान के संशोधनवाद का मुक़ाबला करने के लिए अपर्याप्त है। पाकिस्तान की धरा से पनप रहे आतंकवाद तथा भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों को अपना समर्थन कम करने में पाकिस्तानी सेना की अनिच्छा पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उदासीनता या जानबूझकर चुप्पी से आहत होकर, नई दिल्ली ने आतंक के विरुद्ध अपनी सैन्य कार्यवाही की सीमा को पुनः परिभाषित किया है| अंततः, 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के उत्तर में, नई दिल्ली ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए नौ सटीक हमले किए, जिसे भारत ने “नपा-तुला, गैर-बढ़ावा देने वाला, आनुपातिक और ज़िम्मेदार कार्यवाही” कहा है। कई दशकों के रणनीतिक संयम की नीति पर क़ायम रहने के उपरांत, पाकिस्तान के उप-परंपरागत छद्म युद्ध के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जांच कराने में भारत के असफल प्रयासों के कारण एक दृढ़ सैद्धांतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है, जो इस सैन्य टकराव से परे भी गूँजेगा।
दंडात्मक सैन्य कार्यवाही के आलोचकों ने प्रायः इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत के ये उपाय पाकिस्तान को इस उप-परंपरागत छद्म युद्ध से पूर्ण रूप से रोकने में असमर्थ हैं। इस हालिया संकट के दौरान भी, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि गतिज कार्यवाही से घरेलू स्तर पर पाकिस्तानी सेना की दुर्बल स्थिति और प्रबल हो सकती है, यद्यपि अस्थायी रूप से। संयम बरतने की हिदायत देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को धीरे-धीरे पाकिस्तान में राजनीतिक परिवर्तन को प्रभावित करना चाहिए। तथापि, पाकिस्तान में आंतरिक परिवर्तन को प्रभावित करने की भारत की क्षमता स्वाभाविक रूप से सीमित है। यदि केवल संयम बरतने से ही पाकिस्तानी सेना की हालत दुर्बल होती या पाकिस्तानी राजनीतिक दलों का सेना के साथ मिलकर “हाइब्रिड शासन” बनाने का निर्बाध सहयोग समाप्त हो सकता, तो भारत यह लक्ष्य पहले ही फ़तह कर चुका होता। बल्कि पाकिस्तान के असैनिक नेतृत्व के साथ सार्थक वार्तालाप के पिछले भारतीय प्रयास—आंशिक रूप से उसकी स्थिति को प्रबल करने हेतु—प्रायः उलटे पड़े हैं, जैसा कि कारगिल युद्ध (1999), मुंबई हमले (2008) और पठानकोट हमले (2016) दर्शित करते हैं। भारत में कई लोग इन घटनाओं को पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत के प्रति अपने देश की नीति में किसी भी बड़े परिवर्तन का विरोध करने हेतु जानबूझकर किए गए अंतर्ध्वंस के रूप में देखते हैं।
कई दशकों के रणनीतिक संयम की नीति पर क़ायम रहने के उपरांत, पाकिस्तान के उप-परंपरागत छद्म युद्ध के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जांच कराने में भारत के असफल प्रयासों के कारण एक दृढ़ सैद्धांतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है, जो इस सैन्य टकराव से परे भी गूँजेगा।
पाकिस्तान के लिए, हालाँकि, यह केवल 2019 में था जब संबंध काफी खराब हो गए, जब भारत ने पुलवामा में 40 भारतीय सैनिकों की हत्या के प्रत्युत्तर में, सीमा पार हवाई हमले किए और उसके बाद भारत-प्रशासित कश्मीर की स्वायत्तता और राज्यत्व का प्रतिसंहरण कर दिया| हालांकि यह मुखर भारतीय दृष्टिकोण नई दिल्ली में वैचारिक मंथन से कम, बल्कि हाल के वर्षों में विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने के प्रयास में जोखिम उठाने में पाकिस्तानी असैन्य नेताओं की अक्षमता या अनिच्छा से अधिक अवतरित हुआ है (परवेज़ मुशर्रफ से लेकर नवाज़ शरीफ़ तक), जो कुछ हद तक पाकिस्तानी सेना द्वारा लगाई गई बाधाओं के कारण है। इसलिए, जबकि भारतीय नेतृत्व ने सदैव एक मुखर दृष्टिकोण की हिमायत की है, वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के प्रति भारत की हालिया “प्रबल” और प्रतिभूतिकृत रणनीति एक केंद्रित कूटनीतिक प्रयासों के बाद उभरी है|
भविष्य के संकटों के लिए अतीत से सबक
अतीत के झरोखे से, 2013 की घातक झड़पों और युद्धविराम उल्लंघनों में वृद्धि के बावजूद, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने पाकिस्तानी समकक्ष को आमंत्रित किया। सार्थक वार्ताओं का परिणाम 2015 में एक संयुक्त वक्तव्य था जिसमें दोनों सरकारों ने “सभी लंबित मुद्दों” पर चर्चा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पाकिस्तान 2008 के मुंबई हमलों की सुनवाई में तीव्रता लाने पर सहमत हुआ, जबकि भारत ने कश्मीर मुद्दे पर वार्तालाप के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। द्विपक्षीय अड़चनों और उभरते मतभेदों के बावजूद, मोदी ने पाकिस्तान में सार्क शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के निमंत्रण को स्वीकार किया और पेरिस में सौहार्दपूर्ण बैठक ने बैंकॉक में एनएसए स्तर की बैठक का मार्ग प्रशस्त किया। इस गुप्त पहल के अंतर्गत, भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा कर “आगे बढ़ने” का संदेश दिया, जिससे समग्र द्विपक्षीय संवाद पुनः प्रारंभ हुआ| शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिसंबर 2015 के अंत में शरीफ़ के आवास पर एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोदी द्वारा लाहौर की अभूतपूर्व यात्रा से और भी बल मिला, जबकि इस क़दम की भारतीय विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। हालाँकि, इस साहसिक समझौतापूर्ण पदध्वनि का उत्तर एक सप्ताह के उपरांत पठानकोट में भारतीय वायु सेना के अड्डे पर आतंकवादी हमले के रूप में भारत को मिला|

उस समय जनभावना की अवहेलना करते हुए, भारतीय नेतृत्व ने हमले के संयुक्त अन्वेषण हेतु पाकिस्तान की पेशकश स्वीकार कर ली, जिसके कारण भारत सरकार को राजनीतिक घाटा भी हुआ| एक प्रतिद्वंद्वी ख़ुफ़िया संस्थान को अपने सैन्य इकाई का दौरा करने की अनुमति देना, और फिर उस पर झूठा ऑपरेशन करने का आरोप लगाना, यह एक कारण है कि भारत अब संयुक्त या निष्पक्ष जाँच के प्रस्तावों को तुरंत ख़ारिज कर देता है। पठानकोट के बाद पाकिस्तान से इस प्रकार की पारस्परिक प्रतिउत्तरता में विफलता के कारण भारत को सितंबर 2016 में उरी हमले का बदला लेने के लिए बल प्रयोग करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने सीमापार छापा मारा। इन “शल्यक प्रहारों” ने भले ही एक नई मिसाल क़ायम की हो, लेकिन पाकिस्तान में विभिन्न राजनीतिक समूहों के साथ पाकिस्तानी सेना के लंबे समय से चल रहे संघर्ष ने समय के साथ स्थिति को और ख़राब कर दिया।
2016 के बाद से, भारत-पाकिस्तान के बीच बार-बार होने वाले संकटों ने नई दिल्ली की दुविधा को और बढ़ा दिया है, क्योंकि जहाँ हमलों के बाद द्विपक्षीय वार्ता के प्रयास किए जाते हैं, वहां बार-बार पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके देश के नागरिक नेतृत्व को दरकिनार कर दिया जाता है| नवाज़ शरीफ़ जैसे नेता, जिन्हें भारत में वास्तव में शांति के पक्षधर के रूप में देखा जाता है, को अक्सर उस समय पद से निष्कासित कर दिया गया है जब प्रमुख द्विपक्षीय शांति प्रयास गति पकड़ रहे होते हैं। भारत के लिए, पाकिस्तानी सेना की इच्छा और असैन्य नेताओं की भारत के साथ संबंधों में बेहतरी लाने की क्षमता प्रत्येक सुनियोजित सत्ता परिवर्तन के साथ क्षीण होती जा रही है| इसके अतिरिक्त, पाकिस्तानी राजनेताओं ने स्वयं यह सुनिश्चित कर लिया है कि वार्ता रियायतों पर ही निर्भर रहेगी, फलस्वरूप जनरल क़मर जावेद बाजवा जैसे इच्छुक सेना प्रमुख के लिए भी भारत के साथ सार्थक वार्तालाप की लागत को पूर्ण रूप से अंतर्लीन करना कठिन हो गया था|
वर्ष 2021 के युद्धविराम समझौते ने संभवतः दोनों पक्षों में सामान्यीकरण के पक्ष में मतों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया। यदि इस्लामाबाद ने अपना रुख़ बरकरार रखा होता, तो भारत-प्रशासित कश्मीर में चुनाव और निकटस्थ राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल होना पुनः वार्तालाप का अवसर प्रदान कर सकते थे। परंतु, नए पाकिस्तानी सेना प्रमुख और अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर की नियुक्ति के उपरांत सतत् तनाव में वृद्धि के कारण, भारत रियायतों पर आधारित वार्ता से दूर, सशर्त वार्तालाप के प्रति सतर्क हो गया है।
संबंधों में बढ़ती गिरावट के दायरे
पाकिस्तान “भारतीय आक्रमण” का मुक़ाबला कर गौरवान्वित महसूस करते हुए, यह भी स्वीकार कर सकता है कि भारतीय बल प्रयोग पर कुछ लागत प्रवर्तित करने के बावजूद (जैसे कि प्रारंभिक चरणों में संभावित भारतीय हवाई नुक़सान), उसे अगले संकट में भारत की पारंपरिक श्रेष्ठता से जूझना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने “बल की उपयोगिता” को पुनः खोज लिया है और वह सैन्य प्रभुत्व बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में किए गए प्रारम्भिक हमले घातक और सटीक थे, जिनमें पाकिस्तान के आंतरिक हिस्से भी सम्मिलित है और जो 1971 के युद्ध के बाद से कभी हमलों के शिकार नहीं हुए थे। साथ ही, पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर खतरनाक प्रकृति और जिस आसानी से भारत ने हवाई सुरक्षा को बेअसर किया, इसका विधिवत आंकलन पाकिस्तान सैन्य योजनाकारों द्वारा किया जाएगा—भले ही पाकिस्तानी जनता का वर्तमान मंतव्य उत्साहपूर्ण क्यों न हो |
अनुष्ठानिक संयम से मुक्ति कभी सहज नहीं रही है, परन्तु भारत का दृढ़ संकल्प अब पाकिस्तान के परमाणु ख़तरे को चुनौती देने से आगे निकल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पाकिस्तान की ख़तरनाक दाँवबाज़ी (brinkmanship) रणनीति का अनुकरण करने का प्रयत्न कर रहा है| इसके बावजूद भी, भारत यह विश्वास नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान इस घाटनक्रम के उपरांत अचानक अपना रुख परिवर्तित कर देंगे | ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तानी सेना ने अपनी रणनीति में नरमी लाने या अपने अधिकतमवादी लक्ष्यों का त्याग करने से इंकार किया है, जिसकी वजह से भारत के साथ-साथ स्वयं पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगताना पड़ा है| इस संकट के बाद पाकिस्तानी सेना को आंतरिक रूप से मिलने वाली क्षणिक राहत के बारे में जानते हुए भी, यह मान्यता है कि पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलें इतनी संरचनात्मक हैं कि मध्यम से दीर्घ अवधि में इनका समाधान नहीं हो सकता।
अनुष्ठानिक संयम से मुक्ति कभी सहज नहीं रही है, परन्तु भारत का दृढ़ संकल्प अब पाकिस्तान के परमाणु ख़तरे को चुनौती देने से आगे निकल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पाकिस्तान की ख़तरनाक दाँवबाज़ी (brinkmanship) रणनीति का अनुकरण करने का प्रयत्न कर रहा है|
भविष्य में भारत के लिए विकल्प
प्रत्येक हमले को “युद्ध का कर्त्य” मानने की सार्वजनिक घोषणाओं का पालन करना अपनी अन्तर्निहित चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, परन्तु, नई दिल्ली में यह दृढ़ निश्चय विद्यामान है कि आतंकी हमले के प्रतिउत्तर में बल प्रयोग से पाकिस्तान को गंभीर क्षति पहुँचाई जा सकती है—भले ही ऐसी कार्यवाहियों में कूटनीतिक अथवा अन्य प्रकार के जोखिम अन्तर्निहित क्यों न हो|
हालाँकि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका को लेकर कुछ चिंता है। प्रारंभ में, वाशिंगटन ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को माना, जब उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया उचित है, बशर्ते कि वह सोच-समझकर की गई हो। फिर भी, कई भारतीयों का मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा युद्ध विराम की सार्वजनिक घोषणा ने उस सैन्य लाभ को दुर्बलता प्रदान की जिसे भारत ने नूर खान और सरगोधा वायुसैनिक ठिकानों जैसे वायुसैनिक ठिकानों पर निशाना साधकर हासिल किया था| ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ फोन के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया| जबकि भारतीय अधिकारी मानते हैं कि संघर्ष विराम पर ट्रम्प की अधिकांश घोषणाएं मुख्य रूप से एक “शांति निर्माता” के रूप में उनकी छवि को प्रबल करने के बारे में हैं और ट्रम्प की मध्यस्थता की पेशकश 2019 की तरह ही केवल आकस्मिक टिप्पणियाँ हैं| लेकिन यह जनता के साथ भली भांति प्रतिध्वनित नहीं हुई है।
फिर भी, “पुनः-हाइफ़नेशन” के डर के बारे में चिंता करने के बजाय, भारत अब पाकिस्तान को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता पर अधिक जाँच के लिए दबाव बनाने हेतु अपनी साझेदारियों और बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रभावशाली लाभ उठाने का प्रयास कर सकता है। यहाँ तक कि सिंधु जल संधि पर अस्थायी रोक भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि भारत जल पर वार्ता को आतंकवाद से जोड़ने तथा पाकिस्तान को अलग-थलग करने के पिछले प्रयासों को आगे बढ़ाने पर अड़ा हुआ है।
फिर भी, वैश्विक उथल-पुथल और बीजिंग से उत्पन्न ख़तरों तथा पड़ोस में उसके बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान पर निशाना साधने के लिए अमेरिका जैसे साझेदारों पर दबाव डालना अंततः भारत की प्राथमिकता न हो| हालांकि, जैसे-जैसे यह अनिश्चितता के बादल छंट जाएंगे, भारतीय संस्थापन में इस बात को लेकर आत्ममंथन हो सकता है कि क्या नई दिल्ली एक प्रमुख शक्ति बनने के अपने रास्ते में पाकिस्तान की चुनौती को दरकिनार कर सकता है, विशेषकर तब जब चीन-पाकिस्तान धुरी मज़बूत होती जा रही है।
***
This article is a translation. Click here to read the original in English.
Image 1: César Guillotel via Pexels
Image 2: Raajan via Flickr